
महात्मा गांधी का कथन था कि सत्ता नष्ट और भ्रष्ट करती है। नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि रिटायरमेंट के बाद सब आईएएस संत हो जाते हैं। इधर पिछले दिनों नमामि गंगे से जुडे़ एक शीर्षस्थ आईएएस अधिकारी से मैंने यूं ही पूछ लिया कि गांवों द्वारा किए छोटी नदियों के पुनर्जीवन के कामों से क्या सरकार कुछ सीख सकती है?
"सुनत बचन उपजा मन क्रोधा। माया बस न रहा मन बोधा।"
वह गुस्सा हो गए। उन्होने कहा कि एन जी ओ वाले बाहर बैठकर हल्ला करते रहते हैं; भीतर रहकर पता चलता है। इस पर मैने कहा कि मेरा कोई एन जी ओ नहीं है। मैं एक आज़ाद लेखक-पत्रकार हूं तो उन्होने साफगोई दिखाई - तिवारी जी, मैं सीख सकता हूं; सरकार नहीं। सरकार बहुत बड़ी होती है।
इन सब कड़ियों में बनारस के गांधी विद्या संस्थान की इमारत पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कब्जे की पटकथा को जोड़कर देखें तो प्रमाणित होता है कि जब राज आता है तो उसके साथ राजरोग भी आता है। मात्र इन संदर्भों से ही संकेत मिल जाता हैं कि गांघी विद्या संस्थान कब्जा प्रकरण में कौन-कौन, कहां-कहां और क्यों नष्ट या भ्रष्ट हुआ है। यूं ही नहीं कहा जाता कि सत्ता चाहे परिवार की हो, नगर-गांव-संगठन की, व्यापार की अथवा सरकार की; सत्ता का भाव आ जाने मात्र से ही हम नष्ट और भ्रष्ट होना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार यह सत्ता भाव ही तो है, जिसके कारण सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन के भीतर से लोकतंत्र की रक्षा खातिर खम्भ ठोक कर डट जाने वाले भी निकले तो चारा खाने वाले भी।

राजरोगियों की रज़ामंदी
गांधी मार्ग के संपादक रहे स्वर्गीय श्री अनुपम मिश्र ने नदी जोड़ परियोजना के खिलाफ एक लेख लिखा था। लेख का शीर्षक था - राजरोगियों की रज़ामंदी। लेख की शुरूआत में ही लिखा था कि अच्छे लोग भी जब राज के नज़दीक पहुंचते हैं तो उनको विकास का रोग लग जाता है; भूमंडलीकरण का रोग लग जाता है। उन्होंने इसे प्रमाणित करती एक घटना का जिक्र किया था। घटना यूं थी कि कर्नाटक में वेड़थी नदी पर बांध बनाया जा रहा था। किसानों को आशंका हुई कि बांध बनने से खेती का चक्र बिगड़ जाएगा। उन्होंने डटकर विरोध किया। लगातार पांच साल तक आंदोलन चला। रामकृष्ण हेगड़े, उस आंदोलन के एकछत्र नेता रहे। यह नेता भाव, उन्हे सत्ता में ले आया। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेगडे़ वेड़थी बांध के पक्ष में हो गए।
अनुपम जी ने इसे राजरोग का उदाहरण बताते हुए इस राजरोग का इलाज भी बताया था। लिखा था - हेगडे़ के पाला बदलने के बावजूद किसानों का आंदोलन चलता रहा। हेगडे़ का राज चला गया। उनका राजरोग भी चला गया। आंदोलन के कारण वह बांध आज तक नहीं बन सका।
सम्मेद शिखर, जालियांवाला बाग, साबरमती आश्रम, श्री अरविंद आश्रम (पुदुचेरी), बद्रीनाथ, केदारनाथ - ये सभी हमारी आस्था व विचारों की विरासत के तीर्थ हैं। तीर्थों पर तीर्थभाव को तिरोहित कर पर्यटन बढ़ाने और पैसा कमाने की परियोजना बनाना, एक तरह विकास का राजरोग है। तेज़ हॉर्न की आवाज़ से लुड़क जाने वाली कंकड़ी के नम पहाड़ में वोल्वो दौड़ाने लायक सड़क बनाना सामान्य मनोदशा तो नहीं ही कही जाएगी। पूरे देश में एक ही पार्टी, एक ही रंग और एक ही विचार के लोग राज करेंगे। बाकी को तोड़ना-फोड़ना, दुश्मन मानकर नष्ट करने पर उतारु हो जाना; यह दूसरे तरह का राजरोग है। ...तो क्या समझें कि जब नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या बीजेपी सरकार में नहीं रहेगी तो यह राजरोग चला जाएगा?

हां, राज जाने से राजरोग भी चला जाता है।
हो सकता है कि बीजेपी केन्द्र की सरकार में न रहे तो गांधी विद्या संस्थान की इमारत, उसे वापस मिल जाए। मोदी नीत सरकार न बताती है और न सुनती है। उसे जो बताना है, वह वही बताती है। उसे जो करना है, वह वही करती है। कहते हैं कि सवालपूछी होने से जवाबदेही आती है। लेकिन वह जवाबदेही की जगह ई डी, सी बी आई, इनकम टैक्स और पुलिस ले आती है। इस डर ने लम्बे समय तक उन सभी को चुप रखा, जिनके जीवन का कुछ न कुछ प्रत्यक्ष तौर पर सरकार के नियंत्रण में हैं। आप राजनेता हैं तो आपको आपकी पिछली फाइल दिखाई जा सकती है। अनुदान आधारित नागरिक संगठन है तो आपको प्राप्त अनुदान और किए खर्च पर जांच बैठाई जा सकती है। आप पत्रकार हैं तो आपके मालिक को धमकाकर आपकी नौकरी छीनी जा सकती है। आप व्यापारी हैं तो आपकी टैक्स फाइल खोली जा सकती है। आप उद्योगपति हैं तो आपके उत्पाद के नमूने उठाकर सही को ग़ल़त बताकर फंसाया जा सकता है। हो सकता है कि मोदी नीत सरकार के जाने से यह डर खत्म हो। बुलडोजर और भरी कोर्ट में गोली की जगह संविधान सम्मत न्याय हो। हो सकता है कि तब गरीब-अमीर की खाई पाटने के कुछ संजीदा प्रयास हों। निजी ठेकेदारी बढ़ाने की जगह, स्थाई रोज़गार सृजित करने की दशा में कुछ कदम आगे बढ़ें। किन्तु क्या इससे राज और राजरोग चला जाएगा?
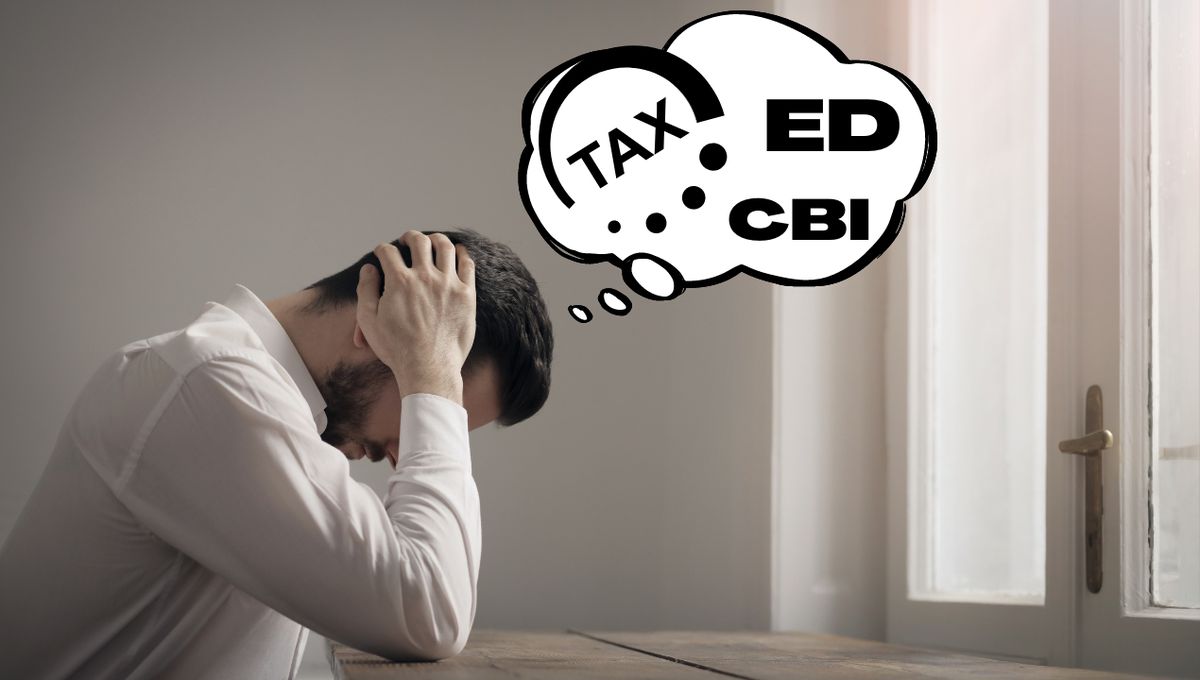
क्या हो राजरोग मिटाने का औजार ?
कोई कह सकता है कि राज जाने का मतलब, किसी व्यक्ति या दल का सरकार से हट जाना हो है। आजकल प्रयास भी यही चल रहा है। देश का एक बड़ा वर्ग एकजुट हो रहा है। राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं। नागरिक संगठनों में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी दलों में खडे़ हैं और सर्व समुदाय के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन भी। पत्रकारों में भी लामबंदी नज़र आ रही है। यह सारी लामबंदी एक ही सूत्र पर आधारित है कि 2024 में मोदी को सत्ता से हटाना है। क्या वोट ही राजरोग दूर करने का एकमात्र औजार है?
सोचिए कि यदि गांधी जी जिंदा होते तो क्या वह भी यही करते या वह कहते - "नहीं भाई, इससे बात नहीं बनेगी। दलों के पक्ष-विपक्ष में खडे़ होना, वोटर का काम है। वह करे।" जब मैं खुद जनप्रतिनिधियों को जनता से कटे तथा ऐसे व्यवहार करते देखता हूं कि जैसे वे किसी अन्य लोक के प्राणी हों तो यह विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाता है कि बात बनेगी तो मुद्दे के पक्ष-विपक्ष में कमर कसकर खड़ा हो जाने से। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि राजरोग खत्म हो।
मेरी राय है कि किसी व्यक्ति अथवा दल के आने-जाने से राजरोग की पकड़ कमज़ोर अथवा मज़बूत तो पड़ सकती है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती। सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद कांग्रेस गई; जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आई। क्या हुआ? यदि राजरोग को जड़ से निपटाना है तो इस राज और नेता...दोनों के भाव को ही लोकतंत्र से हमेशा के लिए बाहर करना होगा। राजनीति और राजनेता - राज का भाव पैदा करते हैं। इसका इससे अधिक पुख्ता प्रमाण क्या हो सकता है कि जो स्वयं प्रतिनिधि हैं, उन हमारे सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र में सांसद प्रतिनिधि नियुक्त कर लिए हैं। स्पष्ट है कि राजनीति और राजनेता को हटाकर लोकनीति और लोकप्रतिनिधि वाले भाव के लिए जगह बनानी होगी।
नेता नहीं, प्रतिनिधि बनाइए
हमें खुद समझना होगा कि नेता अगुवा होता है। उसके पीछे उसके अनुयायी होते हैं। नेता जो कहता है, अनुयायी वह करते हैं। लोकप्रतिनिधि अगुवा नहीं होता। लोकप्रतिनिधि, लोगों द्वारा लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना अथवा नामित किए जाता हैं। प्रतिनिधि का काम होता है कि वह जिनका प्रतिनिधि है, उनके निर्णय की पालना करे। उनके विचार को... प्रस्ताव को आगे बढ़ाये। उनकी आवाज़ को पुरजोर तरीके से जहां उठाना है; उठाये। अतः हमें अपने प्रतिनिधियों को नेता, राजनेता व अधिकारी कहना बंद करना होगा। वह समझें कि विधायी, शासकीय अथवा प्रशासनिक कार्य के लिए इलेक्ट अथवा सेलेक्ट होना, राजयोग नहीं है। यह जनसहयोग है।

विधायी प्रतिनिधि सभाओं की बात करूं तो लोकनीति और लोकप्रतिनिधित्व के भाव के मार्ग में एक बड़ी बाधा चुनावों का दलगत होना है। चुनावों के दलगत् होने ने सामुदायिक भाव व सद्भाव को बुरी तरह तोड़ दिया है। चुनावी मशीनों पर से दलों के निशान हटा देने चाहिए। चुनावी व्यवस्था तोड़क की बजाय, जोड़क कैसे बने; ऐसे बदलाव करने चाहिए। हमारे पंच, प्रधान, विधायक व सांसद इन्हे चुनने वाले लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। किन्तु सदन में पहुंचकर लोगों के ये प्रतिनिधि, दलों के प्रतिनिधि के तौर पर व्यवहार करते हैं। दलगत् व्हिप जारी करने का प्रावधान, बची-खुची संभावना को नष्ट कर देता है। हमें समझना चाहिए कि जिन्हे लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया, वे लोगों के प्रतिनिधि हैं। मंत्री-प्रधानमंत्री सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।
अतः बाध्य करना होगा कि इन सभी को क़ानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया जाये; ताकि ये लोक, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधि रहते हुए किसी दल के निशान, बैठक, पद, चंदा व प्रचार में हिस्सेदार न बने। वोटरों को अपने चुने प्रतिनिधि पर दबाव बनाना होगा कि वह प्रतिनिधि पद की शपथ लेने से पहले दल की बुनियादी सदस्यता से इस्तीफा दे। साथ ही साथ हमें लोक उम्मीदवार, लोक घोषणापत्र, लोक नियोजन, लोक अंकेक्षण और लोक निगरानी तंत्र के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी रखनी चाहिए। पंचायत व नगर निगम/पालिका के स्तर पर वार्ड सभाओं का गठन कर उन्हे प्रतिनिधियों पर नियंत्रण व उसे सहयोग की जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित करना चाहिए। हमें ऐसे हस्तक्षेप करने होंगे, ताकि प्रतिनिधि के अधिकार वैयक्तिक न होकर, जिसके वे प्रतिनिधि हैं, उस संस्था के सांस्थानिक हों। ये हस्तक्षेप, राजरोग को नष्ट करने का योग साबित हो सकते हैं।
यह कैसे होगा?
अनुपम मिश्र फिर मार्गदर्शन करते हैं। वह लिखते हैं कि यह दौर बहुत विचित्र है। इस दौर में सब विचारधारायें ओर हर तरह के राजनैतिक नेतृत्व में रजामंदी है विनाश के लिए। इस सर्वसम्मति के बीच हमारी आवाज़ दृढ़ता और संयम से उठनी चाहिए। जो बात कहनी है, वह दृढ़ता से कहनी पडे़गी। हमें प्रेम से कहने का तरीका निकालना पडे़गा। हमें अब सरकार का पक्ष समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे समझने में लगे तो ऐसी भूमिका हमें थका देगी। हम कोई पक्ष जानना नहीं चाहते। हम कह सकते हैं कि यह पक्षपात है देश के साथ, भूगोल के साथ, इतिहास के साथ। इसे रोको।
प्रश्न है कि हम ऐसा हम कब कह सकेंगे?
अत्यंत प्रबुद्ध और गंभीर पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी ने एक पोर्टल पर लिखे लेख में बनारस के गांधी वालों द्वारा चार कसमें खाने का उल्लेख किया है। गांधी, खादी और समाजसेवी संस्थाओं को सामने रखूं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा वे तब कह सकेंगे, जब इनके संचालक बिना कसम खाए ही आइने को अपनी ओर घुमा लेंगे। तय करेंगे कि पद, पैसे और सुविधा के लोभ में इन्हे गांधी, खादी और सेवा कर्म का सत्यानाश नहीं करना चाहिए। जरूरी खर्च के लिए धन का इंतज़ाम किसी फंडिग एजेन्सी से नहीं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य समूह से और अपने श्रम से अर्जित करेंगे।
सामाजिक कार्य में कोई अधिकारी व कर्मचारी नहीं होता; सब समान सम्मानित कार्यकर्ता होते हैं। अंतिम बात यह कि एकादश व्रत को सिर्फ पढे़ या पढ़ायेंगे नहीं, अपनाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। आखिरकार, अपने अंतिम वक्त तक महात्मा गांधी भी तो यही कर रहे थे। कांग्रेस को लोक सेवक संघ के रूप में रूपांतरित कर गांधी भी तो सत्ता भाव को तिरोहित करना चाहते थे। गांधी, इसीलिए तो खास थे, चूंकि वह वही कहते थे, जिसे वह बेहिचक कर सकते थे। किन्तु गांधी विद्या संस्थान ने अब तक यह नहीं किया। अब करे।
इन सब बातों को मुझसे ज्यादा बेहतर, रामबहादुर राय खुद जानते हैं। वह कभी जनसत्ता में प्रभाष जोशी जैसे प्रखर संपादक के प्रखर सहयोगी रहे हैं। गांधी, विनोबा, जे पी और कृपलानी से लेकर मोदी मानस की अच्छी समझ रखते हैं। कम खर्च में जीवन चलाने में यकीन रखते हैं। अब उन्हे तय करना है कि वह विनोबा की मान भूदान से प्रेरित हों; ज़मीन को लेने का प्रस्ताव वापस लें। गांधी को मानकर सत्य के पक्ष में खडे़ हो जायें। पश्चाताप् करें, कुर्सी छोड़ें। गांधी-विनोबा-जे पी की विरासत को आगे ले जाने में सबसे आगे नज़र जायें अथवा अपने अगले कदम के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र का नाम बदलकर अटल बिहारी बाजपेई जी के नाम को आगे बढ़ाने में जुट जायें। कला केन्द्र को हिंदू राष्ट्र अध्ययन केन्द्र बनायें। राजरोगी कहलायें।
''नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं, प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।''
................................................................................






 tag on profile.
tag on profile.
By Arun Tiwari {{descmodel.currdesc.readstats }}
Arun Tiwari {{descmodel.currdesc.readstats }}
महात्मा गांधी का कथन था कि सत्ता नष्ट और भ्रष्ट करती है। नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि रिटायरमेंट के बाद सब आईएएस संत हो जाते हैं। इधर पिछले दिनों नमामि गंगे से जुडे़ एक शीर्षस्थ आईएएस अधिकारी से मैंने यूं ही पूछ लिया कि गांवों द्वारा किए छोटी नदियों के पुनर्जीवन के कामों से क्या सरकार कुछ सीख सकती है?
वह गुस्सा हो गए। उन्होने कहा कि एन जी ओ वाले बाहर बैठकर हल्ला करते रहते हैं; भीतर रहकर पता चलता है। इस पर मैने कहा कि मेरा कोई एन जी ओ नहीं है। मैं एक आज़ाद लेखक-पत्रकार हूं तो उन्होने साफगोई दिखाई - तिवारी जी, मैं सीख सकता हूं; सरकार नहीं। सरकार बहुत बड़ी होती है।
इन सब कड़ियों में बनारस के गांधी विद्या संस्थान की इमारत पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कब्जे की पटकथा को जोड़कर देखें तो प्रमाणित होता है कि जब राज आता है तो उसके साथ राजरोग भी आता है। मात्र इन संदर्भों से ही संकेत मिल जाता हैं कि गांघी विद्या संस्थान कब्जा प्रकरण में कौन-कौन, कहां-कहां और क्यों नष्ट या भ्रष्ट हुआ है। यूं ही नहीं कहा जाता कि सत्ता चाहे परिवार की हो, नगर-गांव-संगठन की, व्यापार की अथवा सरकार की; सत्ता का भाव आ जाने मात्र से ही हम नष्ट और भ्रष्ट होना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार यह सत्ता भाव ही तो है, जिसके कारण सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन के भीतर से लोकतंत्र की रक्षा खातिर खम्भ ठोक कर डट जाने वाले भी निकले तो चारा खाने वाले भी।
राजरोगियों की रज़ामंदी
गांधी मार्ग के संपादक रहे स्वर्गीय श्री अनुपम मिश्र ने नदी जोड़ परियोजना के खिलाफ एक लेख लिखा था। लेख का शीर्षक था - राजरोगियों की रज़ामंदी। लेख की शुरूआत में ही लिखा था कि अच्छे लोग भी जब राज के नज़दीक पहुंचते हैं तो उनको विकास का रोग लग जाता है; भूमंडलीकरण का रोग लग जाता है। उन्होंने इसे प्रमाणित करती एक घटना का जिक्र किया था। घटना यूं थी कि कर्नाटक में वेड़थी नदी पर बांध बनाया जा रहा था। किसानों को आशंका हुई कि बांध बनने से खेती का चक्र बिगड़ जाएगा। उन्होंने डटकर विरोध किया। लगातार पांच साल तक आंदोलन चला। रामकृष्ण हेगड़े, उस आंदोलन के एकछत्र नेता रहे। यह नेता भाव, उन्हे सत्ता में ले आया। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेगडे़ वेड़थी बांध के पक्ष में हो गए।
अनुपम जी ने इसे राजरोग का उदाहरण बताते हुए इस राजरोग का इलाज भी बताया था। लिखा था - हेगडे़ के पाला बदलने के बावजूद किसानों का आंदोलन चलता रहा। हेगडे़ का राज चला गया। उनका राजरोग भी चला गया। आंदोलन के कारण वह बांध आज तक नहीं बन सका।
सम्मेद शिखर, जालियांवाला बाग, साबरमती आश्रम, श्री अरविंद आश्रम (पुदुचेरी), बद्रीनाथ, केदारनाथ - ये सभी हमारी आस्था व विचारों की विरासत के तीर्थ हैं। तीर्थों पर तीर्थभाव को तिरोहित कर पर्यटन बढ़ाने और पैसा कमाने की परियोजना बनाना, एक तरह विकास का राजरोग है। तेज़ हॉर्न की आवाज़ से लुड़क जाने वाली कंकड़ी के नम पहाड़ में वोल्वो दौड़ाने लायक सड़क बनाना सामान्य मनोदशा तो नहीं ही कही जाएगी। पूरे देश में एक ही पार्टी, एक ही रंग और एक ही विचार के लोग राज करेंगे। बाकी को तोड़ना-फोड़ना, दुश्मन मानकर नष्ट करने पर उतारु हो जाना; यह दूसरे तरह का राजरोग है। ...तो क्या समझें कि जब नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या बीजेपी सरकार में नहीं रहेगी तो यह राजरोग चला जाएगा?
हां, राज जाने से राजरोग भी चला जाता है।
हो सकता है कि बीजेपी केन्द्र की सरकार में न रहे तो गांधी विद्या संस्थान की इमारत, उसे वापस मिल जाए। मोदी नीत सरकार न बताती है और न सुनती है। उसे जो बताना है, वह वही बताती है। उसे जो करना है, वह वही करती है। कहते हैं कि सवालपूछी होने से जवाबदेही आती है। लेकिन वह जवाबदेही की जगह ई डी, सी बी आई, इनकम टैक्स और पुलिस ले आती है। इस डर ने लम्बे समय तक उन सभी को चुप रखा, जिनके जीवन का कुछ न कुछ प्रत्यक्ष तौर पर सरकार के नियंत्रण में हैं। आप राजनेता हैं तो आपको आपकी पिछली फाइल दिखाई जा सकती है। अनुदान आधारित नागरिक संगठन है तो आपको प्राप्त अनुदान और किए खर्च पर जांच बैठाई जा सकती है। आप पत्रकार हैं तो आपके मालिक को धमकाकर आपकी नौकरी छीनी जा सकती है। आप व्यापारी हैं तो आपकी टैक्स फाइल खोली जा सकती है। आप उद्योगपति हैं तो आपके उत्पाद के नमूने उठाकर सही को ग़ल़त बताकर फंसाया जा सकता है। हो सकता है कि मोदी नीत सरकार के जाने से यह डर खत्म हो। बुलडोजर और भरी कोर्ट में गोली की जगह संविधान सम्मत न्याय हो। हो सकता है कि तब गरीब-अमीर की खाई पाटने के कुछ संजीदा प्रयास हों। निजी ठेकेदारी बढ़ाने की जगह, स्थाई रोज़गार सृजित करने की दशा में कुछ कदम आगे बढ़ें। किन्तु क्या इससे राज और राजरोग चला जाएगा?
क्या हो राजरोग मिटाने का औजार ?
कोई कह सकता है कि राज जाने का मतलब, किसी व्यक्ति या दल का सरकार से हट जाना हो है। आजकल प्रयास भी यही चल रहा है। देश का एक बड़ा वर्ग एकजुट हो रहा है। राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं। नागरिक संगठनों में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी दलों में खडे़ हैं और सर्व समुदाय के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन भी। पत्रकारों में भी लामबंदी नज़र आ रही है। यह सारी लामबंदी एक ही सूत्र पर आधारित है कि 2024 में मोदी को सत्ता से हटाना है। क्या वोट ही राजरोग दूर करने का एकमात्र औजार है?
सोचिए कि यदि गांधी जी जिंदा होते तो क्या वह भी यही करते या वह कहते - "नहीं भाई, इससे बात नहीं बनेगी। दलों के पक्ष-विपक्ष में खडे़ होना, वोटर का काम है। वह करे।" जब मैं खुद जनप्रतिनिधियों को जनता से कटे तथा ऐसे व्यवहार करते देखता हूं कि जैसे वे किसी अन्य लोक के प्राणी हों तो यह विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाता है कि बात बनेगी तो मुद्दे के पक्ष-विपक्ष में कमर कसकर खड़ा हो जाने से। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि राजरोग खत्म हो।
मेरी राय है कि किसी व्यक्ति अथवा दल के आने-जाने से राजरोग की पकड़ कमज़ोर अथवा मज़बूत तो पड़ सकती है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती। सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद कांग्रेस गई; जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आई। क्या हुआ? यदि राजरोग को जड़ से निपटाना है तो इस राज और नेता...दोनों के भाव को ही लोकतंत्र से हमेशा के लिए बाहर करना होगा। राजनीति और राजनेता - राज का भाव पैदा करते हैं। इसका इससे अधिक पुख्ता प्रमाण क्या हो सकता है कि जो स्वयं प्रतिनिधि हैं, उन हमारे सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र में सांसद प्रतिनिधि नियुक्त कर लिए हैं। स्पष्ट है कि राजनीति और राजनेता को हटाकर लोकनीति और लोकप्रतिनिधि वाले भाव के लिए जगह बनानी होगी।
नेता नहीं, प्रतिनिधि बनाइए
हमें खुद समझना होगा कि नेता अगुवा होता है। उसके पीछे उसके अनुयायी होते हैं। नेता जो कहता है, अनुयायी वह करते हैं। लोकप्रतिनिधि अगुवा नहीं होता। लोकप्रतिनिधि, लोगों द्वारा लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना अथवा नामित किए जाता हैं। प्रतिनिधि का काम होता है कि वह जिनका प्रतिनिधि है, उनके निर्णय की पालना करे। उनके विचार को... प्रस्ताव को आगे बढ़ाये। उनकी आवाज़ को पुरजोर तरीके से जहां उठाना है; उठाये। अतः हमें अपने प्रतिनिधियों को नेता, राजनेता व अधिकारी कहना बंद करना होगा। वह समझें कि विधायी, शासकीय अथवा प्रशासनिक कार्य के लिए इलेक्ट अथवा सेलेक्ट होना, राजयोग नहीं है। यह जनसहयोग है।
विधायी प्रतिनिधि सभाओं की बात करूं तो लोकनीति और लोकप्रतिनिधित्व के भाव के मार्ग में एक बड़ी बाधा चुनावों का दलगत होना है। चुनावों के दलगत् होने ने सामुदायिक भाव व सद्भाव को बुरी तरह तोड़ दिया है। चुनावी मशीनों पर से दलों के निशान हटा देने चाहिए। चुनावी व्यवस्था तोड़क की बजाय, जोड़क कैसे बने; ऐसे बदलाव करने चाहिए। हमारे पंच, प्रधान, विधायक व सांसद इन्हे चुनने वाले लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। किन्तु सदन में पहुंचकर लोगों के ये प्रतिनिधि, दलों के प्रतिनिधि के तौर पर व्यवहार करते हैं। दलगत् व्हिप जारी करने का प्रावधान, बची-खुची संभावना को नष्ट कर देता है। हमें समझना चाहिए कि जिन्हे लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया, वे लोगों के प्रतिनिधि हैं। मंत्री-प्रधानमंत्री सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।
अतः बाध्य करना होगा कि इन सभी को क़ानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया जाये; ताकि ये लोक, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधि रहते हुए किसी दल के निशान, बैठक, पद, चंदा व प्रचार में हिस्सेदार न बने। वोटरों को अपने चुने प्रतिनिधि पर दबाव बनाना होगा कि वह प्रतिनिधि पद की शपथ लेने से पहले दल की बुनियादी सदस्यता से इस्तीफा दे। साथ ही साथ हमें लोक उम्मीदवार, लोक घोषणापत्र, लोक नियोजन, लोक अंकेक्षण और लोक निगरानी तंत्र के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी रखनी चाहिए। पंचायत व नगर निगम/पालिका के स्तर पर वार्ड सभाओं का गठन कर उन्हे प्रतिनिधियों पर नियंत्रण व उसे सहयोग की जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित करना चाहिए। हमें ऐसे हस्तक्षेप करने होंगे, ताकि प्रतिनिधि के अधिकार वैयक्तिक न होकर, जिसके वे प्रतिनिधि हैं, उस संस्था के सांस्थानिक हों। ये हस्तक्षेप, राजरोग को नष्ट करने का योग साबित हो सकते हैं।
यह कैसे होगा?
अनुपम मिश्र फिर मार्गदर्शन करते हैं। वह लिखते हैं कि यह दौर बहुत विचित्र है। इस दौर में सब विचारधारायें ओर हर तरह के राजनैतिक नेतृत्व में रजामंदी है विनाश के लिए। इस सर्वसम्मति के बीच हमारी आवाज़ दृढ़ता और संयम से उठनी चाहिए। जो बात कहनी है, वह दृढ़ता से कहनी पडे़गी। हमें प्रेम से कहने का तरीका निकालना पडे़गा। हमें अब सरकार का पक्ष समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे समझने में लगे तो ऐसी भूमिका हमें थका देगी। हम कोई पक्ष जानना नहीं चाहते। हम कह सकते हैं कि यह पक्षपात है देश के साथ, भूगोल के साथ, इतिहास के साथ। इसे रोको।
प्रश्न है कि हम ऐसा हम कब कह सकेंगे?
अत्यंत प्रबुद्ध और गंभीर पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी ने एक पोर्टल पर लिखे लेख में बनारस के गांधी वालों द्वारा चार कसमें खाने का उल्लेख किया है। गांधी, खादी और समाजसेवी संस्थाओं को सामने रखूं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा वे तब कह सकेंगे, जब इनके संचालक बिना कसम खाए ही आइने को अपनी ओर घुमा लेंगे। तय करेंगे कि पद, पैसे और सुविधा के लोभ में इन्हे गांधी, खादी और सेवा कर्म का सत्यानाश नहीं करना चाहिए। जरूरी खर्च के लिए धन का इंतज़ाम किसी फंडिग एजेन्सी से नहीं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य समूह से और अपने श्रम से अर्जित करेंगे।
सामाजिक कार्य में कोई अधिकारी व कर्मचारी नहीं होता; सब समान सम्मानित कार्यकर्ता होते हैं। अंतिम बात यह कि एकादश व्रत को सिर्फ पढे़ या पढ़ायेंगे नहीं, अपनाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। आखिरकार, अपने अंतिम वक्त तक महात्मा गांधी भी तो यही कर रहे थे। कांग्रेस को लोक सेवक संघ के रूप में रूपांतरित कर गांधी भी तो सत्ता भाव को तिरोहित करना चाहते थे। गांधी, इसीलिए तो खास थे, चूंकि वह वही कहते थे, जिसे वह बेहिचक कर सकते थे। किन्तु गांधी विद्या संस्थान ने अब तक यह नहीं किया। अब करे।
इन सब बातों को मुझसे ज्यादा बेहतर, रामबहादुर राय खुद जानते हैं। वह कभी जनसत्ता में प्रभाष जोशी जैसे प्रखर संपादक के प्रखर सहयोगी रहे हैं। गांधी, विनोबा, जे पी और कृपलानी से लेकर मोदी मानस की अच्छी समझ रखते हैं। कम खर्च में जीवन चलाने में यकीन रखते हैं। अब उन्हे तय करना है कि वह विनोबा की मान भूदान से प्रेरित हों; ज़मीन को लेने का प्रस्ताव वापस लें। गांधी को मानकर सत्य के पक्ष में खडे़ हो जायें। पश्चाताप् करें, कुर्सी छोड़ें। गांधी-विनोबा-जे पी की विरासत को आगे ले जाने में सबसे आगे नज़र जायें अथवा अपने अगले कदम के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र का नाम बदलकर अटल बिहारी बाजपेई जी के नाम को आगे बढ़ाने में जुट जायें। कला केन्द्र को हिंदू राष्ट्र अध्ययन केन्द्र बनायें। राजरोगी कहलायें।
................................................................................
Attached Images