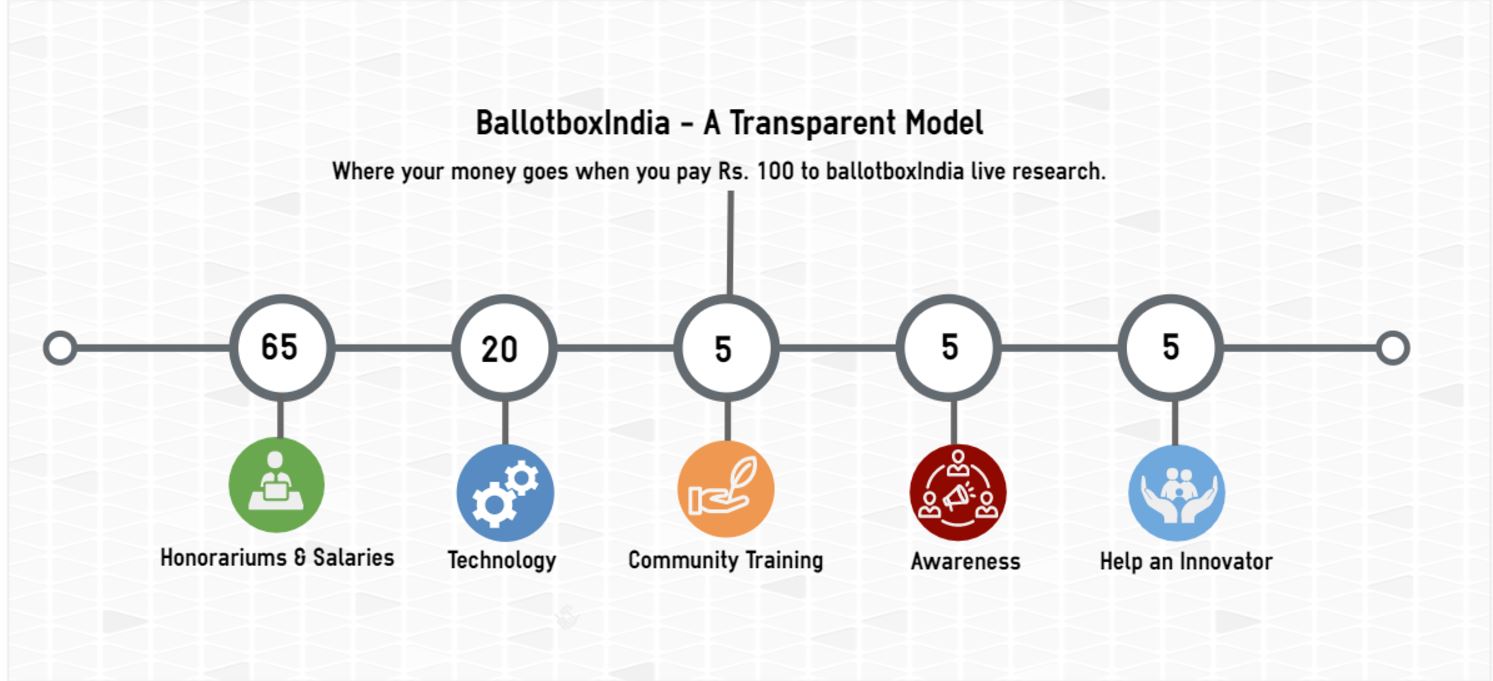पुरानी पत्रकारिता (ओजी) एवं प्रगतिशील यानि नव पत्रकारिता (पीजी), दो सिद्धांतो का संघर्ष का संघर्ष है. इन सिद्धांतो के अंतर्विरोध और गूगल इत्यादि के ज़माने में आज जो वैचारिक मिलावट आ गई है, यक़ीनन चर्चा का विषय है, आप चाहे तो आज की प्राइम टाइम खबरों पर नजर डाल सकते हैं.
देखिये, प्राइम टाइम का बड़ा महत्व है, दस साल पहले शायद
इतना ना हो, मगर आज प्राइम टाइम अपने
मेक या ब्रेक के कगार पर है.
ये आम विचार है कि - मीडिया कॉर्पोरेट अधीन है, पेड पत्रकारिता अपने चरम पर है या कुछ जर्नलिस्ट
भ्रष्ट हैं और कुछ भले, सब TRP का खेल है, लाभ-उन्माद है, ये डिबेट तो सौ साल से भी ऊपर से चली आ रही है.
फ़िल्में, कम से कम गुरुदत्त की समाज का आइना मानी जा सकती हैं, 1956 में फिल्म “प्यासा” में अख़बार/पत्रिका के
मालिकों ने गुरुदत्त का जो हाल किया था, उससे मीडिया में भ्रष्टाचार कोई नई घुट्टी
नहीं है. इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है.


तो आज और बीते कल में क्या अंतर है?
पहले प्राइम टाइम 8-9 के बीच का समय होता था, “ आप शम्मी नारंग से समाचार सुन रहे हैं, या “ये आकाशवाणी है, पेश हैं आज के समाचार” ख़बरें बिना किसी भावनाओं के पेश की जाती थी, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, कोई सनसनी नहीं. कुछ
नेशनल न्यूज़, कुछ लोकल खबरें, पूरा परिवार, मित्र साथ बैठ कर देखते थे, सुनते थे. चौपालें सजती थी, आमने सामने बातचीत होती थी.
अगली सुबह चाय के स्टालों पर उन्हीं ख़बरों पर
अख़बार पढ़ चर्चा की जाती थी. चाय और कॉफ़ी हाउस, कचोरी सब्जी की दुकानें, ख़बरों पर व्यूज या
समझ बनाने के काम आती थी. कुछ विशेषज्ञ हुआ करते थे, जिनके एडिटोरियल हुआ करते थे. कुछ लोग उनको पढ़ बाकि लोगों को समझाते थे, डिबेट लोकल हुआ करती थी.
तब भी कॉरपोरेट मीडिया था, विज्ञापन बेस्ड टेबलायड अख़बार थे, पेनी जर्नलिज्म था. पोपुलर कल्चर या पुराने समय के मीडिया
को भी देखे तो भ्रष्ट पत्रकार और अख़बार वाले कई जगह भ्रष्ट नेताओं के साथ लिप्त
दिखाए गए.

*1981 में बनी राष्ट्रीय
फिल्म विकास निगम की ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक होने के साथ उस समय की सोच भी बताती
थी. पत्रकारों को लगातार कई बार भ्रष्ट बताया जाता रहा है.
1984 के सिख दंगो और
इमरजेंसी के दौरान भी सरकारी मीडिया, जैसे दूरदर्शन और आकाशवाणी का इस्तेमाल
प्रोपगंडा फ़ैलाने में किया गया, ऐसा
लगातार बोला जाता रहा है.
प्रिंट मीडिया काफी हद तक सरकारी दबाव से मुक्त
माने जाते हैं, मगर राजनीतिक शक्तियों
द्वारा पत्रकारों को डराना, धमकाना, विज्ञापन का लालच देकर अपनी तरह से न्यूज़ बनवाना काफी सुनने
में आता था.
कल भी पत्रकार अपनी पॉलिटिकल मेल जोल या “लायसनिंग” के हिसाब से स्टोरीज
करते थे, तब भी लेफ्ट और राईट सोचने
वाले पत्रकार होते थे, एक डैम से बिजली और
फायदे गिनता था तो दूसरा हमेशा विस्थापना, खेती की बर्बादी इत्यादि की बात बोलता था. कोई युद्ध की लालसा रखता था तो कोई
सैनिकों के परिवारों की भी बात कहता था.
तो आज और कल में क्या बदला, क्यों आज ओजी और पीजी के अपने अलग अलग मीडिया के
तरीकों पर एक चर्चा ज़रूरी है ?
फर्क आया है, एक बड़ा ही धीमा मगर मज़बूत फर्क.
इसको हम हरित
क्रांति से जोड़ेंगे, हरित क्रांति का कांसेप्ट
एक पाक साफ़ कांसेप्ट था, मगर जो बिना
प्लानिंग या एक बहुत टूटी फूटी प्लानिंग के साथ, इंसानी लालच को भड़का कर दशकों तक किया गया. उसने आज किसानी और ज़मीन का जो हाल
किया है, वो जग जाहिर है.
पंजाब की कैंसर वाली ट्रेन हो या पेस्टिसाइड से
भरे हुए खाद्य पदार्थ या भूजल रहित होते खेत, आत्महत्या करते किसान आज भारत में ये सब संसाधनों के अति दोहन और महालाभ
उन्माद से सीधा जोड़ा जाता रहा है. इस कहानी के पीछे भी बड़ी देसी विदेशी पेस्टिसाइड
और फ़र्टिलाइज़र कंपनिया रही हैं, जिन्होंने स्थानीय
एजेंट्स के साथ मिल कर किसानों को इस लालच के जाल में फंसा कर इस हालत पर पहुंचा
दिया.
तो क्या आज की पत्रकारिता भी उसी तरह के लालच और
उलझन के दौर से गुज़र रही है जो शायद उसे पूरी तरह बदल कर रख देगी, शायद अस्तित्व ही खत्म हो जाए.
इनफार्मेशन बूम की ऊँची लहर पर चढ़ सबसे ज्यादा
फ़ायदा कमाने के चक्कर में घुस तो गए, मगर क्या अब ये लहर इतनी मज़बूत है कि इनको चला रही है, बहाती ले जा रही है और शायद पता नहीं कहाँ ले जा कर पटके
फर्क आया है..
पहला फर्क ये आया है कि पहले सूचना और जानकारी एक पहचाने चेहरे से दूसरे पहचाने चहरे तक
जाती थी, न्यूज़, व्यूज और भावनाएं अलग अलग रहती थी, अलग अलग समय पर लोगों तक पहुँचती थी. काफी कम फ्रीक्वेंसी
में लोगों तक पहुंचती थी, लोगों की समझ बनाने
में आमने सामने की डिबेट का हाथ भी होता था और सूचना फर्स्ट लेवल रिसर्च होती थी.
गौर से देखें तो आज के 24 घंटे न्यूज़ चैनल, क्या एक ही न्यूज़ को बना बना कर बार बार अलग अलग तरह से ही नहीं दिखाते. जी, आप सही समझे 24 घंटे की न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले ब्रेक नहीं करेंगे तो जैसे न्यूज़ दूध की तरह फट
जाएगी.
*एक मुख्य चैनल की ब्रेकिंग
न्यूज़
समाज में न्यूज़ बढ़ी नहीं है, न्यूज़ उतनी ही है, मगर न्यूज़ वालों ने न्यू “न्यूज़ बनाने” की कला सीख ली.
* वायरल कर देने की ललक, एक दूसरा न्यूज़ चैनल. ये गिरावट कहाँ थमेगी कहा नहीं जा
सकता.
एक बड़ा अंतर आप तब और अब में देखें
शम्मी नारंग यानि दूरदर्शन की ख़बरों से पहले
चित्रहार आता था, यानि न्यूज़ के लिए अलग
सेक्शन, मनोरंजन के लिए अलग, अलग से न्यूज़ चैनल की जरूरत नहीं थी. अख़बार एक मुख्य माध्यम
थे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे
टीवी और रेडियो न्यूज़ को एक सेक्शन की तरह दिखाते थे. मूक बधिरों के लिए भी एक
सेक्शन होता था, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और न्यूज़ अलग अलग सेक्शन में और अलग अलग गरिमा
के साथ दिखाए जाते थे.
आजतक ने इसको तोड़ा 1995 के आस पास, पहली बार रात 10 बजे के बाद, कटे हुए सर और हाथ, चटखारे लेकर एक
मनोरंजक तरीके से बताए जाने लगे. आजतक के सामने पुराने तरीकों ने घुटने टेक दिए, ये वो ग्लोबलाइजेशन का समय था. खुला बाज़ार, खुली सोच, खुला लाभ अपने पूरे
जोर पर था.
किसी समझदार ने सोचा की अगर एक घंटे में इतना
लाभ तो 24 घंटे में कितना. बस
शुरू हुआ सनसनी पे सनसनी का दौर. ये न्यूज़ को न्यूज़ की तरह सुनाने की परंपरा पर
पहली चोट थी.
पत्रकार और उनके पूर्वाग्रह, भावनाएं कभी न्यूज़ में सामने नहीं आते थे, ये गरिमा जब टूटी तो बड़ा फ़ायदा हुआ.
* खबरें रचनात्मक होने लगी, चंद्रकांता फॉर्मेट में खबरें एक न्यूज़ चैनल पर.
24 घंटे के न्यूज़ में
एक मौलिक ख़ामी है - चित्रहार, पारिवारिक सीरियल और
कुछ मसालेदार कार्यक्रमों की कमी पूरी करनी पड़ती है. तो ख़बरें भी उसी अंदाज़ में
फ़ैल गयी, कभी सास बहु के अंदाज़ में, तो कभी रियल्टी ड्रामा के अंदाज़ में, सेलेब्रिटी का पीछा करने में, कभी न्यूज़ एंकर चित्रहार की तरह नाच नाच कर न्यूज़ पेश करने लगे, कुछ तो अदालत लगाने लगे.
न्यूज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन भारी हो गया, क्या बिकेगा, कौन सा सेगमेंट ख़रीदेगा, आम लोग का प्रोग्राम
या इंटेलेक्चुअल सब अपना अपना मार्केट पकड़ने लगे. नेता अभिनेता सब खींच लिए गए.
राजनीति में भी ड्यूटी लगा दी गयी, सबसे मोटी खाल वाले, ढीट किस्म के मगर
एंटरटेनिंग तरीके से बहस करने वाले प्रवक्ता बना दिया गए.
सबका फ़ायदा, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, पैसे का पैसा.
ड्रामे के बीच नेता जवाब देने से बच गया और अभिनेता अपना प्रोडक्ट भी बेच गया.
जनता को चाहिए मनोरंजन, ब्रेड और सर्कस, सब लगे परोसने में.
जो पत्रकार थे, जो खबर चेक करते थे, यथोचित श्रम, फैक्ट चेक इत्यादि करता थे, जो “गेटकीपर” या ख़बरों का द्वारपाल थे, वो खत्म हो गए. इस नयी पीढ़ी के चीखते चिल्लाते, ड्रामा करते “फेस लेस”, “नेम-लेस” (बिना चेहरे और बेनाम सूत्रों) “खबरें बेचते” न्यू मीडिया के सामने सब फेल.
ये खेल चलता रहा, पुराने और नए मीडिया के बीच
लड़ाई चलती रही, कुछ पुराने पत्रकार अपनी
गरिमा संभल कर फिर भी टिके रहें.
ये पुराने पत्रकार बड़ी ही गरिमा के साथ सड़कों पर
निकल जाते थे, साइकिल चलाते हुए, एक पत्रकारिता का नया ही रूप. भावनाएं स्टूडियो में नहीं
प्रत्यक्ष मुद्दों पर आमने सामने.
अंधे लाभ और पेशे की गरिमा - इसकी लड़ाई तो जग जाहिर है, सदियों से चलती आ
रही है. टीवी को अख़बार तो अख़बार को रेडियो. थोडा बैक्टीरिया, थोडा वायरस, थोड़ी हल्दी, थोडा गुड सब एक दूसरे को
काटते रहते थे, कभी कोई आगे तो कभी कोई.
स्थिति बिगड़ रही थी, संभल रही थी.
मुद्दा ये था की लोगों के घर में टीवी नहीं होते
थे, ये 1997 का समय था कुछ संभ्रांत घरों में ही चलता हुआ टीवी होता था, दूरदर्शन तब भी मुख्य चॉइस थी, एंटीना लगाओ और
देखो.
1995 से 2000 की शुरुआत तक भी लोकल रेडियो या अख़बार ही खबरों को पहुंचाते
थे, लोग पढ़ते थे. गाँव बचे हुए
थे, इनफार्मेशन छन कर आती थी.
एडिटर से एडिटर, पत्रकार से पत्रकार.
कुछ शहरी “इन्फेक्टेड” लोग पैसा कमावा दे रहे थे, मगर तब भी केबल टीवी जो इंसान पैसा दे कर ले रहा है, वो
पिक्चर और सीरियल ही देखता था.
मुझे याद है 2000 के आस पास चीज़े बदली, या बदलती हुई दिखीं.
एक नया प्राणी दिखाई देने लगा – इन्टरनेट और उस
पर बैठे कुछ और प्राणी..गूगल, याहू, लाइकोस इत्यादि.
इनपर मनोरंजन का काफी कुछ मिल जाता था. साइबर
कैफ़े में 10 रूपए दो और एक अलग
ही दुनिया. पिक्चर की कहानियां, ज्ञान की बातें
इत्यादि.
2005-2006 तक आते आते इनमें से
एक ही बचा गूगल, गूगल का ई-मेल, गूगल का ऑरकुट, गूगल का मैप, “इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी” सामने खड़ी थी और एक ही जबरदस्त खिलाड़ी था.
गूगल की कहानी हम गूगल बनाम गाँधी में कवर
करेंगे. मगर यहाँ ये जान लेते हैं कि ये सिर्फ़ शुरुआत थी.
तो शुरू करते हैं, उस न्यूज़ या मास मीडिया के
बारे में बात - जो आज यहाँ बौद्धिक रूप से पाताल में पड़ा है और शायद अब उसके पास
इस ICU में ज्यादा समय भी नहीं है.
उस मीडिया के यहाँ तक पहुँचने का.
गूगल 2004 के आस पास संकट में था, सर्च इंजन बनाना कोई
बहुत बड़ी बात नहीं है, dukdukgo जो एक प्रमुख सर्च
इंजन है, एक कंप्यूटर विज्ञानी ने खुद छोटी सी टीम के साथ 2-3 साल में बना दिया और गूगल से उन्नीस नहीं है.
उस समय "याहू" "अलता-विस्टा"
आदि काफी सर्च इंजन हुआ करते थे, काफी कम्पटीशन था, मगर आज सिर्फ गूगल है.
गूगल ने ऐसा क्या किया?
गूगल ने सिर्फ अपने आस पास देखा, देखा एंकर को नाचते हुए, चीखते हुए, TRP और विज्ञापन बेचने
के लिए सारी इंसानियत की दीवारें गिरते हुए. खुला बाज़ार, बेलगाम लाभ.
बेलगाम लाभ-उन्माद, जो सिर्फ इंसान की कुछ कमजोरियों जैसे ईगो, लालच, घृणा, मूढ़ता, तृष्णा और उन्माद पर
प्रहार करता है और उसे लाभ में बदलता है.
*विकृत मानसिकता को टारगेट
या विकृत मानसिकता को बढ़ावा, बहरहाल दोनों एक ही
सिक्के के दो पहलू हैं. जबतक विज्ञापन का पैसा आता रहे. ऐसी हेडलाइंस से आज की खबरें पटी पड़ी हैं.
और यहाँ से शुरू हुआ “एड-सेंस” का ज़माना.
*टाइम्स ऑफ़ इंडिया की
वेबसाइट से - ख़बरों के साथ लगाया गया विज्ञापन (बुझों तो जानें) - हर क्लिक पर
पैसा और कमाई. खबर की गरिमा की कोई परवाह नहीं.
आपने शायद “एड-सेंस” के बारे में दीवारों पर या
छोटे छोटे पर्चों, या “एस.एम.एस” इत्यादि पर लिखा
देखा होगा – घर बैठे पैसे कमाएं, गृहणियां, बेरोजगार बस क्लिक
करें, 2रूपए, 4 रूपए हर क्लिक पर कमाएं.
नीचे 2004 में जारी की गयी इस
रिपोर्ट को देखें
गूगल “एड-सेंस” एक बेहद जटिल तरीके से
चलाया जाता है, इसके पीछे गूगल ही नहीं
बहुत बड़ी बड़ी उसकी एफिलिएट कंपनिया लगी हुई हैं. भारत जैसे देश में कई तरह के महाकाय
रिंग्स ये फ़र्ज़ी क्लिक्स बनवाती हैं और लाभ कमाती रही हैं और इससे सीधे गूगल को
फ़ायदा पहुँचता रहा है.
गूगल ने इस कारोबार को गलत तरीके से लगातार कई
साल चलने दिया, बीच बीच में कुछ हलके फुल्के
प्रयास कर ये बस खानापूर्ति की गयी, मगर वी.पी.एन. के उपयोग और सावधानी के साथ करने पर इसको पकड़ना नामुमकिन है.
इस खेल में कितना पैसा है, इसका अंदाजा लगाने के
लिए इस खबर को पढ़ें जिसमे बताया गया है की कैसे
गूगल ने 2006 में $90 मिलियन का आउट ऑफ़ कोर्ट सेटलमेंट किया था इस धोखाधड़ी के केस में फंसने के बाद. गूगल ने उस साल $13 बिलियन का यानि चौरासी हज़ार करोड़ का कारोबार किया था, जिसका अधिकतम हिस्सा इसी "एड-सेंस" की देन था.
हमारा दावा ये नहीं है की आज भी गूगल यही कर रहा
है, मगर यह है की इंसानी चतुराई
- ख़ासकर भारत में, गूगल के किसी भी बोट से
कहीं बढ़ के है, और इस खेल में गूगल को
जितना लाभ होता है, खुले बाज़ार के सिद्धांतों
के हिसाब से एक "इंसेंटिव फॉर क्राइम" को जन्म देता है. कई अनसुलझे सवाल
हैं, जैसे क्या गूगल ने इतनी
कमाई जो गलत तरीके से की उसको वापस किया, या उसी के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा किया? इन सवालों पर गूगल के ऊपर एक
अंतर्राष्ट्रीय जाँच होनी चाहिए.
जांच इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गूगल इस तरह के
लाभ उन्माद से आज भी बाज़ आता नहीं दीखता, 2006 के $90 मिलियन के
"आउट ऑफ़ कोर्ट" समझौते के बाद भी आज 2017 में यूरोपियन
यूनियन ने गूगल पर $2.5 बिलियन का जुर्माना लगाया है. यानि रूपए 162,500,000,000. भारत जैसे देश में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता. इतना ही
नहीं 2018 में भी यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर $5
बिलियन का जुर्माना लगाया है.
गूगल के लालच और गूगल के अर्थशास्त्र ने विश्व
के लिए कितना खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है, इसपर विस्तार से चर्चा बाद में.
अभी के लिए इतना समझ लें कि अगर किसी साईट पर
कोई जा कर किसी विज्ञापन – जो बहुत आम जन को
शायद पता भी नहीं होगा की विज्ञापन है, को क्लिक करता है, तो गूगल एक मोटा
हिस्सा कमाता है, थोडा उस वेबसाइट वाले को भी
मिलता है.
विश्व में ख़ासकर भारत या इस जैसे “विकासशील” देशों में इस खेल को
बहुत बड़े तरीके से खेला गया है, आज इन्टरनेट पर जो
कचरा है, गलत खबरें, सेक्स और फूहड़ता से भरी क्लिक करने को उकसाती तस्वीरें और
भड़काऊ हेडलाइंस, यूट्यूब पर फैला डिजिटल
कचरा, एक ही खबर को बार बार भड़काऊ
“एंगल” के साथ छापना, ये सब गूगल के इसी लाभ उन्माद का
फल है.
“एड-सेंस” इसी TRP के खेल का अलग रूप
था. गूगल इससे खरबों डॉलर बनाता है और यही पैसा उसको अपने कम्पटीशन और किसी भी तरह
के सामाजिक, कानूनी नियंत्रण से अपने आप
को कोसों दूर रखने में मदद करता है.
एक खबर के मुताबिक़ गूगल ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों
को घूस दे कर अपने लिए सरकारी पालिसी और आम जन को अपने उपयोगकर्ताओं
के “निजता”
से जुड़े सवालों पर
लाभकारी छवि देने वाली रिपोर्ट्स बनवाई.
ये दो इंडस्ट्रीज का कम्पटीशन कह लें या सह
अस्तित्व, मगर दोनों
इंडस्ट्रीज “मास मीडिया” और गूगल में गुत्थम गुत्था शुरू थीं.
शुरुआती टकराव में मीडिया, ओल्ड या न्यू के पास कोई चांस नहीं था. टीवी न्यूज़ और अख़बार
घर परिवार तक सीधे जाते थे, आर्काइवल होता था
फिर भी सरकारी और सामाजिक बंधन- थोड़ा ही सही था.
वही गूगल “एड-सेंस” प्राइवेट तरीके से कब
उपभोक्ता तक पहुंचा, कौन से साइबर कैफ़े में बैठे
किस बच्चे ने क्लिक किया, क्या और कब असर कर
के गायब हो गया किसी को कोई सुराग भी नहीं लगा.
“क्लिक-बेट” की बाढ़ आ गयी, इन्टरनेट भर गया इंसानी कमजोरियों को सीधे टारगेट करने वाले हर तरह के सामन
से. कुटीर उद्योग खुल गए और सब मिलकर लग गए गूगल का साम्राज्य बनाने में. इस टूटते
समाज और बर्बाद होती मानवता का सीधा फ़ायदा गूगल को मिला.
आप गूगल का एंड्राइड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, क्रोम में गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल का ही ईमेल इस्तेमाल करते हैं, गूगल आपके बारे में आपकी पसंद, नापसंद के बारे में सब जनता है. और तो और चीन में बने बेहद
सस्ते एंड्राइड फ़ोन हर हाथ में दे कर तो गूगल के मित्रों ने पूरी दुनिया ही मुट्ठी
में करवा दी है.
न्यूज़ मीडिया वाले बेचारे, सिर्फ कयास लगा सकते हैं. और इसी कारण घुटने टेकना ही
मुनासिब समझा.
गूगल विज्ञापन को जब मर्ज़ी दिखा, जब मर्ज़ी गायब कर सकता था, टारगेट के “रुझान और उसकी
पसंद” का बहाना तो था ही, साथ में “आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस”, “एल्गोरिथम”, “मानवता को सामान मौके”, “सूचना की आजादी” इत्यादि बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल बार बार हर
तर्क में कर लो तो बस “कम्पटीशन” और किसी संज्ञान के परे नेता, अभिनेता, जनता सब कतार में.

*खबरों के साथ "क्लिक
बेट", आज हर अख़बार का ऑनलाइन
पन्ना इसी तरह का है. ये है खबरों पर गूगल की माया.
आज अख़बार के संपादकों और पत्रकारों को देख कर उस
किसान की तस्वीर सामने आती है जो हरित क्रांति के साथ कुछ लाभ कमाने के लिए इन
कंपनियों के चक्कर में फंसे और आज बर्बादी के कगार पर हैं. ठीक वैसे ही जैसे अख़बार
वाले गूगल यूनिवर्सिटी के पढ़े एजेंट्स (एस.इ.ओ., ऑनलाइन मार्केटिंग) के चंगुल में फंस "क्लिक बेट", "रचनात्मक खबरों" के चक्कर में फंसे हैं.
जिस तरह हरित क्रांति में कमीशन एजेंट पूरी तरह
से लाभ उन्माद में लगे, उसी तरह इन्टरनेट जो
कि लगातार अपनी पकड़ भारत पर बनाता जा रहा था, उसपर गूगल और उसके एजेंट/सहभागी कंपनियों का कब्ज़ा बढ़ता गया.
फर्जी और बेकार की क्लिक्स की कमाई और “सबके बारे में सब जान” गूगल के बेहद “सर्जिकल स्ट्राइक” वाले विज्ञापन मार्केटिंग विभागों को लुभाने वाले “बड़े बड़े इंगेजमेंट नंबर्स” बनाने लगे.
चौबीस घंटे का विज्ञापन आधारित मीडिया पंख कटे
पंछी की तरह तड़पने लगा. विज्ञापन का बजट जो अब गूगल की तरफ़ जा रहा था
सबसे पहले कमज़ोर मीडिया वाले जो कि अब बहुतायायत
में थे, इसमें सीधे कूद पड़े. कॉपी पेस्ट न्यूज़, “क्लिक-बेट” बना कर मीडिया की वेबसाइट भी कमाई करने लगी. रिंग पर रिंग
बना वो गूगल की भक्ति में लग गए.
इसका सीधा असर पड़ा मेनस्ट्रीम मीडिया पर, जो अब सीधे गूगल से प्रतिस्पर्धा में था. गूगल जो सीधे
विदेशी कंट्रोल और चलता है, बिना किसी हिचक और
ज़िम्मेदारी के लगातार इस खेल से पैसे बनाता रहा.
इसी बीच गूगल की ही अर्थशाश्त्र पर चलते हुए फेसबुक और ट्विटर जैसी निजी इन्टरनेट कंपनिया भी अरबों डॉलर के
साथ इसी विज्ञापन के मार्केट में कूद पड़े.
मीडिया, नेता, अभिनेता अब सेल्फी की ताकत
जान चुके थे, जल्दी से जल्दी कुछ क्षणिक
लाभ या फिर सिर्फ “फॉरेन मेड” सामान को अपने को सर लगा अपने आप को फॉरवर्ड और कूल साबित
करने की एक जबरदस्त रेस सी चालू हो गयी.
आज भारत का भावनात्मक और व्यावहारिक डेटा जिस
तरह से लगातार विदेश गया है, उससे मास मीडिया की दुर्गति या पूरी तरह गूगल की पराधीनता तय है.
आज डोनाल्ड ट्रम्प के चुनावों पर जिस तरह रूस द्वारा
गूगल, फेसबुक
इत्यादि पर सीमा पार से परोक्ष तरीके से प्रचार कर चुनाव कोटेम्पर या रुख बदलने के आरोप है और उसकी जाँच बहुत ही उच्च स्तरीय सरकारी समिति कर
रही है, इसमें कई बड़े लोगों की
कुर्सियां जा चुकी हैं, और राष्ट्रपति खुद
ज़द में आते नज़र आते हैं. यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की और इशारा करती है.
अमेरिका मज़बूत देश है, कंपनियां उसकी है, पूरा सहयोग देगी.
मगर क्या भारत के बारे में ऐसा कहा जा सकता है.
क्या भारत में ऐसी कोई जांच कभी होगी, जहाँ सारे नेता गूगल, फेसबुक और ट्विटर
जैसे मंचों पर जबरदस्त तरीके से टॉप पोजीशन लेने की होड़ लगा रहे हैं. महाकाय
मीडिया और साइबर सेल कई सौ करोड़ का खर्चा, करोड़ों में अनुयाई, ये कैसे कह सकते हैं
भारतीय चुनाव विदेशी प्रभाव से अछूते हैं?
और जब ये देसी विदेशी “मार्केटिंग” और “पी.आर. उपक्रम” इतनी आसानी से पैसा लेकर बिना किसी ज़िम्मेदारी के इन मंचों
पर कुछ भी कर पा रहे हैं, सरकारें बदल पा रहे
हैं, पालिसी अपने हिसाब से मोड़
पा रहे हैं. तो क्या किसी पत्रकार के पास मौका है, सही तरीके से काम कर पाने का?
आज आम
आदमी सीवर का नाला बन गयी दुर्गन्ध मारती नदी के सामने खड़ा होके सेल्फी खींच रहा
है, क्योंकि फेसबुक पर डालना है, क्योंकि फेसबुक वाले ने अपने विदेशी मालिकों के लाभ के लिए “सेल्फी” ही “विकास और आज़ादी” की प्रतीक है - ऐसी सोच बेचीं गयी है और भारत के नेताओं एवं अभिनेताओं ने अपने
क्षणिक लाभ को देख कर इसमें जम के साथ दिया है.
एक आम पत्रकार जब लगातार सर मार मार कर थक जाता
है तो वो भी इसी क्लिक, लाइक, फॉलो के खेल में लग जाता है. किसी साइबर सेल का हिस्सा बन
जाता है कि कम से कम पैसा तो मिले.
आज 21 सदी के शुरुआत का गुरु तो गुड रह गया, चेला शक्कर ही नहीं और भी क्या क्या हो
गया है.
आज बहुत से पत्रकार जो कभी स्टोरी के लिए जी जान
से जुटे रहते थे, आज ट्विटर फॉर्मेट में
न्यूज़ चलाते मिलते हैं. पता नहीं चलता की ये ट्विटर को चला रहे हैं या ट्विटर इनको चला रहा है.
न्यूज़ को ट्वीट कर देना चलो मान भी लें, मगर ट्वीट के लिए न्यूज़ बनाना इस खेल तो कुछ अलग ही दिशा
में ले गया. ट्विटर गूगल की ही अर्थव्यस्था का एक अंग है, कैलिफ़ोर्निया की सिलिकॉन वैली से आया ये तकनिकी मंच आज
राजनीतिज्ञों और उनके साइबर सेल की पसंदीदा जगह बन गया है और पत्रकार (गूगल
यूनिवर्सिटी से पढ़े मार्केटर) के पढ़ावे में जाने अनजाने इसमें खूब साथ भी देते
हैं. ट्विटर
किस तरह प्रजातान्त्रिक समाज के लिए एक खतरा बन चूका है इसके बारे में यहाँ पढ़ें.
आज पत्रकार गूगल की ही स्पोंसेर्शिप लेकर फेक न्यूज़ पर तंज कसते हुए दिखते हैं, तो मुद्दा बेहद अजीब लगता है.
गूगल आज हर भारतीय कहाँ जाता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, मिलने के बाद क्या
करता है, कितने देर के लिए
मिलता है, जब कहीं जाता है तो क्या खोजता है, कौन से राजनेता को चाहता है, कौन सी खबरें पसंद करता है, सब जानता है. और ये व्यवहारिक डेटा देश के कण्ट्रोल से
बाहर विदेशी एजेंसी के कण्ट्रोल में बड़े आराम से आ सकता है. सौजन्य वर्तमान मीडिया
वालों को. जिन्होंने कुछ पैसों के लिए शायद भारत का भविष्य गूगल जैसी कंपनियों को
बेच दिया है .
जब वो फैक्ट चेक वेबसाइट वालों को बुलाते हैं तो
लगता है कि गूगल के ही एफिलिएट बुला लाये हैं कि थोड़ी नूरा कुश्ती हो जाए. जिसने
मानवता को अपने मायावी पाश में जकड़ रखा है और लगातार जीवन खींचता जा रहा है, वही ढोंग कर रहा है की सारी मानवता को फेक न्यूज़, और इन्टरनेट पर फैले महा कचरे से आज़ाद करवाएगा. और जब ये
फैक्ट चेकिंग एफिलिएट "ओपन स्कीम" इत्यादि की बात करते हैं तो लगता है
ये भारत को नहीं जानते या ये जानते हैं कि सब टेक्निकल खेल है, बोलने पर काटना
मुश्किल है.
समस्या जब ज्यादा गंभीर हो तो हमेशा “बैक टू बेसिक्स” जाना चाहिए, यानी जड़ों तक.
आज अगर मीडिया वाले गूगल, फेसबुक, ट्विटर की भक्ति
नहीं छोड़ते और अपने पेशे के लिए गंभीर नहीं होते तो शायद ये पेशा ही न बचे.
गूगल ने तो लोकल न्यूज़ अपने “बोट” द्वारा लिखवाने की
प्रक्रिया शुरू कर ही दी है और ये शायद पत्रकारिता के अंत की शुरुआत है.
आज पुरानी पत्रकारिता हो या नई..दोनों पर ही आज
गूगल की छाया है. आज राष्ट्रीय न्यूज़ के साथ “क्लिक बेट”, टेबलायड एकदम साथ
साथ, न्यूज़ की गरिमा और संजीदगी
जाए भाड में, लोग अपना मनोरंजन करे,
ज्यादा समय बिताएं, गूगल देवता खुश होंगे.
यही मिलावट हर तरह की न्यूज़ में, अख़बार, टीवी. आज प्राइम
टाइम प्रोग्राम में तो कब कोई न्यूज़ की शक्ल में पानी का फ़िल्टर बेचने लगे, आम आँखों को पता भी न चले.
मगर हमारी समझ से, दोनों रूप की पत्रकारिता भारत
को गूगल की छाया से निकाल भी सकते हैं. भारत का बाज़ार आज पूरा खुला है, हर जगह विदेशी बड़ी बड़ी कम्पनियाँ “ऍफ़. डी. आई.” का नाम लेकर हमारे देश में कचरा डंप, प्राकृतिक संसाधनों
का दोहन, मानव संसाधन को एक सस्ता
मजदूर बना उसको लगातार अपने देश से विरक्त कर रही है. गूगल, फेसबुक इत्यादि उसको
सेल्फी के आगे सोचने नहीं दे रही. सूचना
के अधिकार का ये हाल देख कर तो ऐसा ही
लगता है की आम जन आज "सेल्फीवाद" में कितने मुग्ध है.
ऐसे समय में पुरानी पत्रकारिता को वापस आना होगा
और इन गैर ज़िम्मेदार ताकतों से आज़ादी दिलानी होगी. नहीं तो सॉफ्ट
उपनिवेशवाद या डेटा साम्राज्यवाद जिसके बारे में आज
कई बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है
और इस गुलामी से न तो भगत सिंह निकाल पाएँगे न ही कोई गाँधी जी आएँगे. कोशिश रहेगी
कि ये सूरत बदली जाए, गूगल के लाभ उन्माद
और उसके द्वारा किये गए मानवता के प्रति अपराधों को सामने लाने के लिए ज़मीनी
पत्रकारिता को वापस आना ज़रूरी है. ओजी और पीजी और उनके जैसे और कई ज़मीनी पत्रकार
इसमें बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं.
गूगल आज इतना बड़ा है, इतना प्रभावशाली है और कई नेताओं की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट
इसमें जुडी हुई है, आम जन का क्षणिक लालच, इससे
जुड़ा हुआ है. ऐसे में इस व्यहार को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होगा.
मगर एक शुरुआत की जा सकती है.
- जहाँ तक हो सके ब्राउज़र में मोज़िला का इस्तेमाल करें,
- duckduckgo या इस तरह के सर्च इंजन जो आपको ट्रैक नहीं करते, को सर्च के लिए इस्तेमाल करें.
- कभी भी क्रोम पर लॉग इन रह कर गूगल पर सर्च ना करें. क्रोम पर बिंग वीडियोस देखें तो इन्टरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल सर्च करना या यूट्यूब देखना ठीक रहेगा.
- ध्यान रहे की ऐसा करते समय कभी भी जीमेल पर लॉग इन ना हों.
- अपने फ़ोन पर गूगल लोकेशन हिस्ट्री बंद करना ना भूलें. मैप्स के लिए "ऑफलाइन" मैप्स का इस्तेमाल करें, कई ऐसे सीधा साधे
उपक्रम थे जो मैप्स के कारोबार में थे, जो मैप के बदले में पैसा लेते थे, आपकी निजता से कोई लेना देना नहीं है , जिनको गूगल ने आपके डेटा के लालच में ख़तम कर दिया. याहू इ-मेल का
इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
मुद्दें की बात ये कि अलग अलग कंपनियों से अलग
अलग सेवाएँ लें और अपनी निजता के प्रति सजग रहें. भारत का अपना सर्च इंजन अभी बहुत
दूर है, भारत की तकनीकी फ़ोर्स गूगल
और विदेशी समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं. मगर हम जरुर एक तकनीकी टास्क फ़ोर्स
गठित करना चाहेंगे.
और हाँ, कोई पत्रकार अगर क्लिक बेट बनाता या गूगल, फेक बुक, ट्विटर की सेवा में लगा हुआ दिखे तो उसे ये लेख ज़रूर पढाएं.
 tag on profile.
tag on profile.