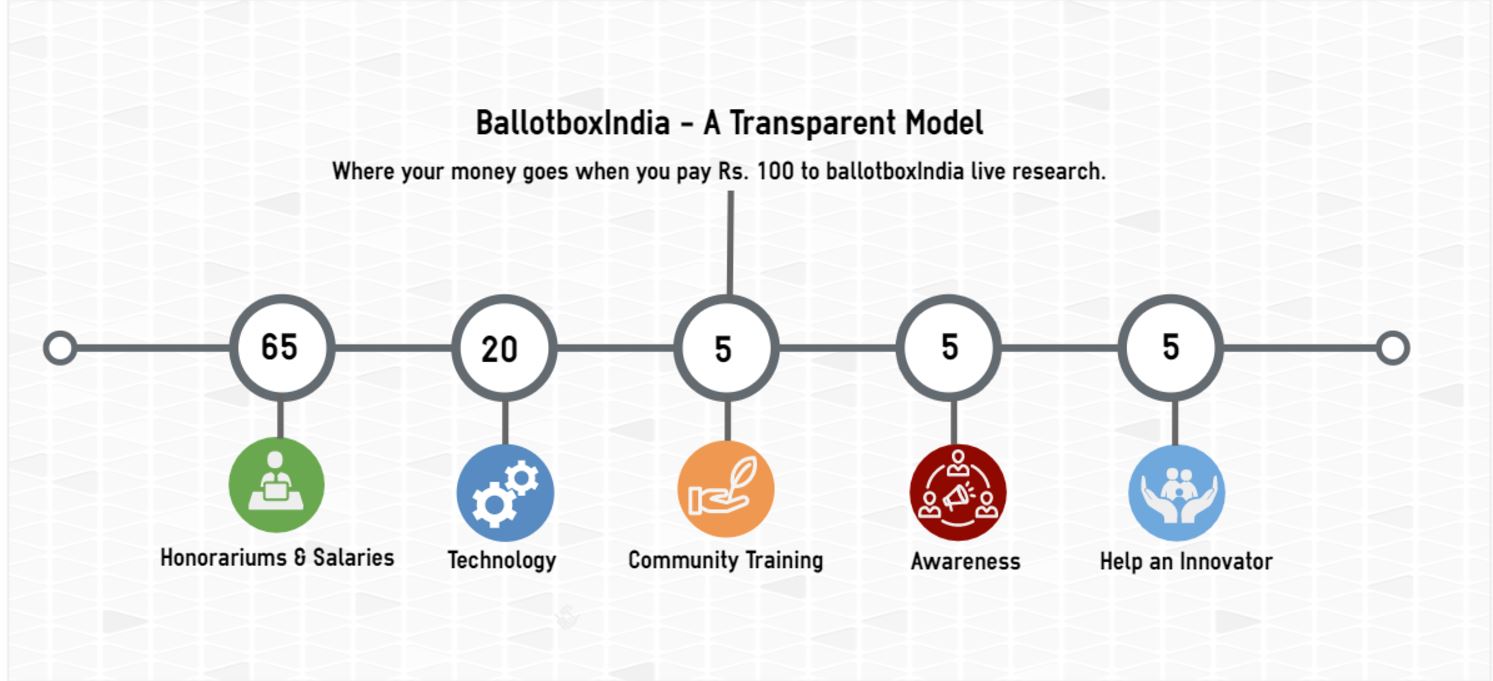Subscribe to this research.
रिसर्च को सब्सक्राइब करें
Join us on the latest researches that matter.
इस रिसर्च पर अपडेट पाने के लिए और इससे जुड़ने के लिए अपना ईमेल आईडी नीचे भरें.

Connect & Follow.
With more and more connecting, the research starts attracting best of the coordinators and experts.

Build a Team
Coordinators build a team with experts to pick up the execution. Start building a plan.

Fix the issue.
The team works transparently and systematically fixing the issue, building the leaders of tomorrow.

जुड़ें और फॉलो करें
ज्यादा से ज्यादा जुड़े लोग, प्रतिभाशाली समन्वयकों एवं विशेषज्ञों को आकर्षित करेंगे , इस मुद्दे को एक पकड़ मिलेगी और तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद ।

संगठित हों
हमारे समन्वयक अपने साथ विशेषज्ञों को ले कर एक कार्य समूह का गठन करेंगे, और एक योज़नाबद्ध तरीके से काम करना सुरु करेंगे

समाधान पायें
कार्य समूह पारदर्शिता एवं कुशलता के साथ समाधान की ओर क़दम बढ़ाएगा, साथ में ही समाज में से ही कुछ भविष्य के अधिनायकों को उभरने में सहायता करेगा।
Communities and Nations where citizens spend time exploring and nurturing their culture, processes, civil liberties and responsibilities. Have a well-researched voice on issues of systemic importance, are the one which flourish to become beacon of light for the world.
समाज एवं राष्ट्र, जहाँ लोग कुछ समय अपनी संस्कृति, सभ्यता, अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने एवं सँवारने में लगाते हैं। एक सोची समझी, जानी बूझी आवाज़ और समझ रखते हैं। वही देश संसार में विशिष्टता और प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं।
Share it across your social networks.
अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर करें
Every small step counts, share it across your friends and networks. You never know, the issue you care about, might find a champion.
हर छोटा बड़ा कदम मायने रखता है, अपने दोस्तों और जानकारों से ये मुद्दा साझा करें , क्या पता उन्ही में से कोई इस विषय का विशेषज्ञ निकल जाए।
Got few hours a week to do public good ?
Join the Research Action Group as a member or expert, work with the right team and make impact. To know more contact a Coordinator with a little bit of details on your expertise and experiences.
क्या आपके पास कुछ समय सामाजिक कार्य के लिए होता है ?
इस एक्शन ग्रुप के सहभागी बनें, एक सदस्य, विशेषज्ञ या समन्वयक की तरह जुड़ें । अधिक जानकारी के लिए समन्वयक से संपर्क करें और अपने बारे में बताएं।
Know someone who can help?
क्या आप किसी को जानते हैं, जो इस विषय पर कार्यरत हैं ?
Invite by emails.
ईमेल से आमंत्रित करें
Code# 6{{ agprofilemodel.currag.id }}
 tag on profile.
tag on profile. का निशान देखें.
का निशान देखें.