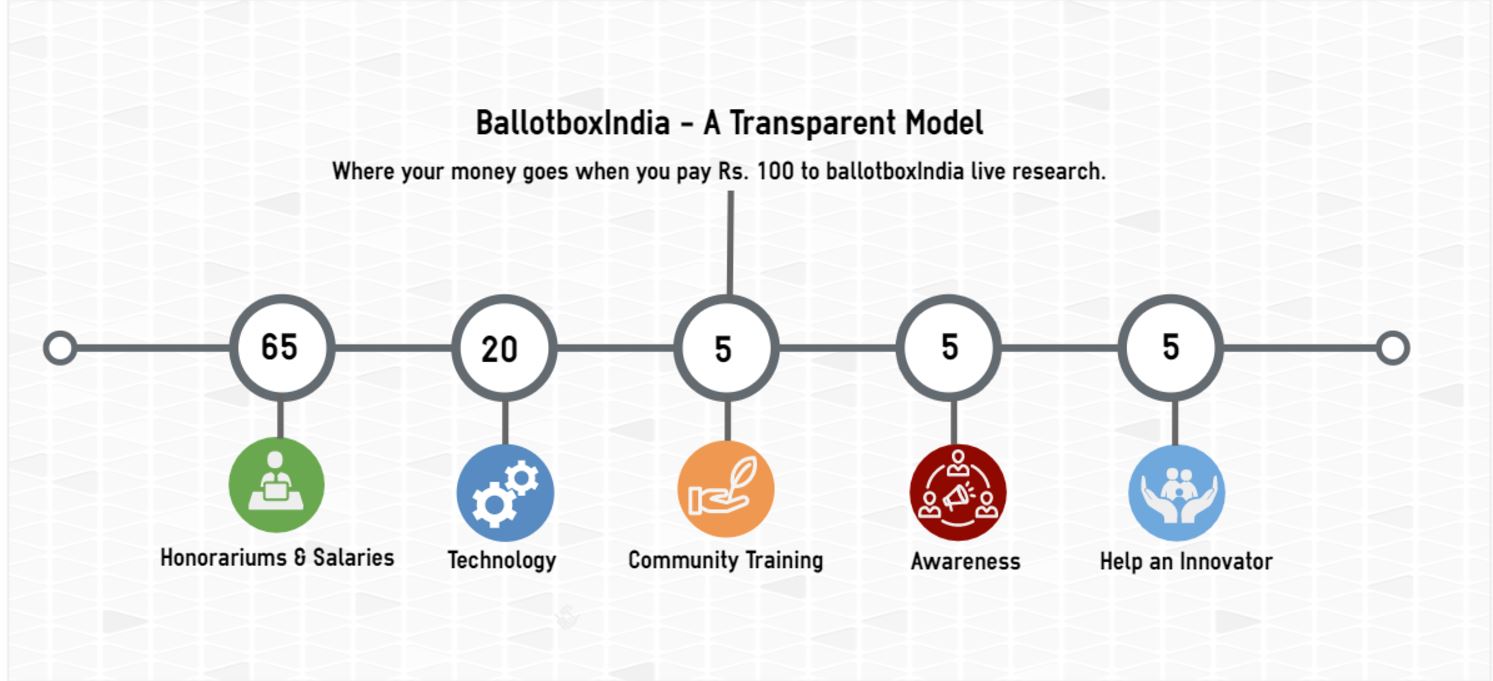"छत्तीसगढ़ के फेफड़े" के रूप में जाना जाता है, हसदेव अरण्य, जो मध्य भारत में 170,000 हेक्टेयर को कवर करने वाले सबसे बड़े अक्षुण्ण सघन वन क्षेत्रों में से एक हैं। यह वन समृद्ध जैव विविधता से समृद्ध है और वनस्पतियों व जीवों की 450 से भी अधिक प्रजातियों का घर है। हाथियों का कॉरिडर और माईग्रेटरी पक्षियों की मेहमाननवाजी करता हसदेव अरण्य छतीसगढ़ के लिए हरियाली के उपहार की तरह है। विभिन्न आदिवासी समुदायों की लोक संस्कृति यहां सदियों से पोषित होती आई है, यहां तक कि हसदेव बांगो बैराज का कैचमेंट क्षेत्र होने के चलते यहां से छत्तीसगढ़ की लगभग चार लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंची जाती है। यहां से निकलने वाली हसदेव नदी गंगा की प्रमुख सहायक महानदी की सहायक धारा है लेकिन जल-जंगल-जीवन के इतने महत्वपूर्ण इस अरण्य के सामने कुछ वर्षों से औद्योगिक कोरोना का संकट खड़ा हुआ है।
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हरा भरा हसदेव अरण्य जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब तक सुरक्षित था लेकिन छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनते ही पूँजीपतियों की नजर भी इस पर आ टिकी। कुछ वर्ष पूर्व जैसे ही यह खबर प्रकाश में आई कि हसदेव जंगल में एक बिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक काला सोना यानि कोयला छिपा हुआ है, देश के कॉर्पोरेट घरानों की दिलचस्पी भी एकाएक हसदेव अरण्य में बढ़ गई।
देश के बड़े उद्योगों की कंपनियां ओपनकास्ट माइनिंग के माध्यम से कोयले के भंडार से परिपूर्ण इस जंगल को नष्ट करने के लिए कमर कस चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक से उत्खनन के लिए कंपनी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिल चुकी है। हालांकि लगभग 2000 एकड़ में विस्तृत परसा कोल ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आबंटित हुआ है लेकिन इसके खनन से जुड़ी प्रक्रिया का अधिकार भारत के एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के पास है। सघन वन क्षेत्र होने के चलते इस कोल ब्लॉक के आबंटन का शुरू से विरोध हो रहा है और यहां निवास करने वाला आदिवासी समुदाय इस निर्णय का विरोध करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। बीते 14 अक्टूबर से आदिवासी धरना-प्रदर्शन के जरिए अपने वन्य क्षेत्र को बचाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं।
जानिए कैसे संकट में है आदिवासी समुदायों की आजीविका, लोक संस्कृति और जीवनशैली
जून, 2020 में जब सारी दुनिया कोरोना से उपजे वैश्विक संकट से दो चार हो रही थी और पर्यावरण की महत्ता समझ रही थी, उस समय कोयला मंत्रालय की पहल पर परसा कोल ब्लॉक में खनन के लिए कोयला नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत होने को थी। अपने अरण्य क्षेत्र पर औद्योगिक प्रगति का खतरा मंडराते देखकर क्षेत्र के नौ ग्राम प्रधानों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रस्तावित खनन नीलामी का विरोध जताया, यहां तक कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र में खनन पर पाबंदी लगाने की भी मांग की।
लेकिन 2009 में "केंद्रीय वन पर्यावरण एवं क्लाईमेट चेंज मंत्रालय" के द्वारा जिस क्षेत्र को "नो-गो" घोषित कर खनन से बचाने की बात कही गई थी और आदिवासी समुदायों द्वारा इसे बचाने के तमाम प्रयास भी किए गए.. उन सभी पक्षों को दरकिनार करते हुए 17 जून, 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया का आरंभ यह कहते हुए किया कि, "यह कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से बाहर निकालने जैसा होगा।"
सघन जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र हसदेव अरण्य का कोयला क्षेत्र 1,879.6 वर्ग किलोमीटर (रायपुर से आठ गुना अधिक क्षेत्रफल) में फैला है और इसमें 23 कोल ब्लॉक शामिल हैं। मुमकिन है कि कोयला आयात में कदम आगे बढ़ाने से देश की अर्थव्यवस्था विकास करे, लेकिन उस सदियों पुरानी लोक संस्कृति, वन्य संपदा का क्या, जो इस विकास के चलते विनाश की ओर खिसकती जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार भले ही कोयला क्षेत्र के लॉकडाउन को मुक्ति मिले, पर क्या इस औद्योगिक विकास रूपी कोरोना से छतीसगढ़ का यह श्वसन तंत्र खोखला नहीं हो जाएगा।
देखें कैसे शुरू हुई इस सघन वन क्षेत्र को उजाड़ने की कहानी..
1.) अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा ईस्ट एंड कांता बसन को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड के हवाले कर दिया था।
2.) जून, 2011 में केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के फॉरेस्ट पैनल ने इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से अहम मानते हुए खनन की सिफारिश के खिलाफ रिपोर्ट पेश की।
3.) तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश ने समिति के निर्णय को नहीं मानकर राज्य सरकार की खनन सिफारिश को स्वीकार किया व अपेक्षाकृत कम घने और कम जैव विविधता वाले क्षेत्र को खनन के लिए अनुमति दे दी।
4.) 2014 में राज्य सरकार के इस निर्णय को एनजीटी में चुनौती दी गई और आरआरवीयूएनएल द्वारा किए जा रहे खनन को स्थगित किया गया। आदेश के तहत आईसीएफआरई के अध्ययन की बात भी कही गई।
5.) स्थानीय समुदायों का विरोध इस दौरान यहां लगातार जारी रहा। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन से लेकर उच्च अधिकारियों तक पत्राचार तक के प्रयास जारी रहे।
6.) 2019 तक भी आईसीएफआरई का अध्ययन क्षेत्र में शुरू नहीं हुआ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर अंतत: मई 2019 में संस्था ने अपना काम शुरू किया। फरवरी 2021 में नौ महीने के अध्ययन के बाद संस्था ने अपनी रिपोर्ट जिन बिंदुओं को रखा, वह इस प्रकार हैं..
- खनन प्रक्रिया से जंगल के मध्यम क्षेत्र की सघनता समाप्त हो जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव वन्य जीवन के आवागमन पर पड़ेगा।
- इस क्षेत्र की संवेदनशील जलवायु भी खनन प्रक्रिया से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, जिससे घुसपैठिए प्रजाति की वनस्पतियों को स्थापित होने में सहायता मिलेगी।
- खनन से मूलभूत ढांचे में भी परिवर्तन आएगा, जिसका असर प्राकृतिक आवास पर पड़ेगा।
- हाथी बहुल क्षेत्र होने के चलते खनन प्रक्रिया से इंसान और हाथियों के बीच का संघर्ष भी बढ़ सकता है।
- खनन की प्रक्रिया से जंगल की काफी जमीन गैर वन्य क्षेत्र के रूप में उपयोग में लाई जाएगी, जिसका व्यापक असर आस पास प्रवाहित होने वाली छोटी नदियों/नालों पर पड़ेगा, जो बड़ी नदियों के लिए जल का प्राथमिक या माध्यमिक स्त्रोत हैं।
- क्षेत्र का लगभग 90 फीसदी आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए खेती या जंगल से मिलने वाले वनोपज पर आश्रित है। खनन के चलते इस समुदाय को विस्थापित करने से इनकी सदियों से पोषित हो रही संस्कृति पर संकट आ जाएगा।
किंतु रिपोर्ट के अंतर्गत इन नकारात्मक बिंदुओं के साथ साथ यह भी कहा गया कि क्षेत्र के चार प्रखंडों यानि कि तारा, परसा, पीईकेबी और केंते विस्तार जैसे कुछ खनन क्षेत्र, जहां खनन शुरू हो चुका है या फिर अनुमति के अंतिम चरण में है, वहां जैव विविधता संरक्षण के प्रबंध कर खनन प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है। यानि अध्ययन में एक ओर जहां खनन से होने वाले नुकसान का जिक्र है तो वहीं दूसरी ओर खनन की सिफारिश भी। जिसे लेकर यह रिपोर्ट विवादों में घिरी रही और इसे आलोचना का शिकार भी होना पड़ा।
जारी है आदिवासी समुदाय का संघर्ष
हसदेव अरण्य में स्थानीय गोंड, पंडों और कोरवा समुदाय अपने वन, वन्य जीवन, लोक संस्कृति और आजीविका को बचाने के लिए तकरीबन दस वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिक विकास व राजनीतिक स्वार्थ के बीच आदिवासी समुदायों की आवाज को दबाया जाना भी निरंतर जारी है। ओपन कास्ट माइनिंग ने एक ओर जहां जंगल, नदियों, वन्य जीवन और आदिवासियों की रोजी रोटी को प्रभावित किया है वहीं उनकी सदियों पुरानी लोकसंस्कृति व जीवनशैली पर भी इसका असर पड़ रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा हसदेव जंगल में तीस कोयला भंडारों को चिन्हित किए जाने के बाद से यानि 2013 से ही खनन प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है, जो परसा पूर्वी कांता बसन में निर्बाध रूप से जारी भी है। तभी से आदिवासी समुदाय भी विरोध का स्वर उठाए हुए हैं। "हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति" के अंतर्गत खदानों के आस पास रहने वाले आदिवासियों ने एकत्रित होकर आंदोलन की शुरुआत की हुई है।
समय बीता, सरकारें बदली, लेकिन आदिवासियों की चिंता आज भी वही है। उन्हें न ही "वन अधिकार कानून" से कोई सुरक्षा मिल पाई और न ही राज्य सरकार का बदलाव होने से। आदिवासी परिवारों के लिए उनका आवास और महुआ, तेंदू पत्ता, चिरौंजी, साल, मशरूम, आग की लकड़ी आदि के तौर पर उनकी जीविका का सबसे बड़ा स्त्रोत धीरे धीरे उनकी ही पहुँच से दूर होता जा रहा है। इसीलिए हसदेव क्षेत्र के 40 गांवों से आदिवासी समुदाय बीते सात वर्षों से 2000 एकड़ में फैले हसदेव को बचाने के लिए आंदोलन में जुटे हैं।
बेतहाशा कोयला खनन से कैसे झारखंड के गिरीडीह शहर का रंग रूप बदल गया, उसके गवाह हम सभी है। कैसे हरियाली भरे इस क्षेत्र से स्पंज आयरन की कंपनियों का धुआं उड़ता नजर आता है, जो दिन में भी रात का आभास देता है। निरंतर होते औद्योगिक विकास से पर्यावरण का जो विनाश गिरीडीह में हुआ, वह आज स्थानीय लोगों में अस्थमा, न्यूमोनिया, टीबी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है।
प्राकृतिक तौर पर आती संवेदनशील जोन में आने वाले उत्तराखंड में नई नई बड़ी परियोजनाएं आती जा रही है, जिनको लेकर अक्सर पर्यावरणविद सरकार को चेताते भी रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे सामने चमोली ग्लेशियर जैसी दुर्घटनाएं आती रहती हैं। विकास के मॉडल को इकोनॉमी, इकोलॉजी, पोलिटिकल, एनर्जी इत्यादि सभी पहलुओं पर तो देखा जाता है लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से देखना उचित नहीं समझा जाता।
तो क्या अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हसदेव अरण्य की नियति भी झारखंड, उत्तराखंड की तरह होगी, क्या महाराष्ट्र की बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बलि दिए जा रहे हजारों मैंग्रोव के वृक्षों की भांति हसदेव के वृक्षों को भी विकास की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। बड़े औद्योगिक घरानों के पास ताकत है, पैसा है लेकिन मात्र 40 गाँव के इन आदिवासियों के पास तो इन जंगलों का ही सहारा है, जिससे इन्हें साल के कुछ 50-60 हजार रुपये अपना जीविका चलाने के लिए मिल जाते हैं।
औद्योगिक विकास हर देश के लिए जरूरी है, लेकिन यदि उसके लिए कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है तो यह हर उस व्यक्ति के लिए सोचने का विषय है जो खुली हवा में सांस ले रहा है और पानी पीकर जिंदा है। सोचिए कहीं देर ना हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो रहे जंगल, सूखती नदियां, घटती वनस्पति, बदलती जलवायु.. यह सभी संकेत हैं कि आने वाला समय हर दिन एक नया संकट लेकर आएगा। सोचिए क्योंकि आप सोचते रहेंगे तो ही "हसदेव_ बचेगा_देश_बचेगा"


 tag on profile.
tag on profile.